केशव तिवारी
साहित्य,
किसी ‘अंधे’ या ‘गए से गए’ दौर में से भी अपने लिए कुछ रोशनियाँ चुन ही लेता है |
यहाँ तक कि , उस दौर से भी , जिसमें सभी धारायें – वे चाहें मुख्य हों या गौड़ -
विध्वंसकारी दिशा में ही बहती दिखाई देती हों | मसलन , ‘केशव तिवारी’ की इस कविता
को देखिये | मुग़ल काल के जिस दौर में अन्य धर्मावलम्बियों के पूजा स्थलों को तोड़ने
के ‘फरमान’ और ‘आदेश’ सर्वत्र दिखाई देते हैं , उसी दौर में से यह कविता ( औरंगजेब का
मंदिर) , किसी मंदिर के निर्माण और उसे सहायता देने का एक
विस्मयकारी ‘फरमान’ ढूंढ लाती है | इसी कविता को केंद्र में रखकर हिंदी के प्रख्यात
आलोचक ‘अजय तिवारी’ ने यह लेख लिखा है , जिसमे इस कविता
के लिखे जाने की स्थितियों के साथ-साथ , उसके भविष्यकालीन महत्व का रेखांकन भी दर्ज
है |
तो प्रस्तुत
है सिताब दियारा ब्लाग पर प्रख्यात आलोचक अजय तिवारी का यह लेख
‘औरंगजेब का मंदिर’
जी हाँ , यह उलटबांसी नहीं है |
पंद्रह बरस पुरानी बात होगी | तब केदारनाथ
अग्रवाल जीवित थे | बांदा में हर साल उनके जन्मदिन पर आयोजन होता था | पहली अप्रैल
के उस सम्मान समारोह में मैं शायद एक दशक बाद गया था | सन 1986 में सम्मान
:केदारनाथ अग्रवाल का एक भव्य समारोह हुआ
था | उसके बाद कई बरस तक बांदा जाने का सुयोग नहीं हुआ था | लेकिन बांदा-वासियों
ने यह सिलसिला टूटने नहीं दिया | आखिर 1997 में आयोजकों की और उससे अधिक केदार की
ईच्छा का सम्मान करते हुए वहां जाना अनिवार्य हो गया | दिल्ली से हमारे आत्मीय
नीरज कुमार और कवयित्री निर्मला गर्ग ने भी केदार के प्रति अपने सहज आदर भाव के
कारण जाने का निर्णय किया था |
केदार पर आयोजन और वह भी बांदा में , उसे सजीव
और महत्वपूर्ण होना ही था | उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था बांदा वासी कवि-मित्र केशव
तिवारी का आग्रह कि चित्रकूट दर्शन कर लीजिये | यह कैफियत जरुरी नहीं है , कि
आस्थावान केशव भी नहीं हैं | लेकिन तुलसीदास और बाल्मीकि का रमणीय प्रदेश , सुन्दर
प्रकृति और गुप्त गोदावरी की रोमांचक गुफा , सच पूछिए तो एक दिन चित्रकूट के लिए
कम पड़ता था | धार्मिक-स्थलों पर पर्यटन के लिए जाना दिलचस्प होता है |
फिर भी इस अत्यल्प समय में भी सार्थकता का
विचित्र-बोध हुआ | दिन रामनवमी का था | मंदिरों में काफी भीड़भाड़ थी | एक मंदिर
काफी पुराना सा , कुछ अलग-थलग और बिलकुल खाली सा था | अन्दर जाकर देखा तो ‘प्रसाद’
की तैयारी थी , लेकिन प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्त नहीं थे | हम सबने तय किया कि
यहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे |
पुजारियों से बातचीत में पता चला तो आश्चर्य का
ठिकाना न रहा , कि यह मंदिर मुग़ल शासक औरंगजेब का बनवाया हुआ है |
एक फ्रेम में औरंगजेब का शाही फरमान मढ़ा हुआ सुरक्षित
है , जिस पर अंग्रेजी राज्य में खास कार्यवायी नहीं हुयी | आजादी के बाद कुछ
सरकारी सहायता मिली , लेकिन अपर्याप्त | मुग़ल शासन के बाद इस मंदिर के अच्छे दिन
नहीं लौटे |
संभवतः हिंदी अकादमी , दिल्ली से प्रकाशित
‘औरंगजेब के फरमान’ (संपादक: डा.विश्वम्भर नाथ पाण्डेय ) में यह दस्तावेज मौजूद हो
| मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सका हूँ |
जिन्हें पता है , वे जानकार उस ओर जाते नहीं ,
कि औरंगजेब का (बनवाया) मंदिर है , और प्रान्त या केंद्र की सरकारें विशेष मदद
करती नहीं | हमारे लिए यह जानकारी दिलचस्प और विचारोत्तेजक थी | उतना ही विचित्र
था यह अनुभव कि चित्रकूट में स्थित एक मंदिर कितना उपेक्षित हो सकता है , उसके
पुजारी और महंथ कितने बेचारे हो सकते हैं |
बांदा से चित्रकूट की यात्रा में आते और जाते
हुए केशव तिवारी ने कुछ दूसरों की और बहुत सी अपनी कवितायें सुनायी | उन पर चर्चा
हुयी | खास तौर पर जो बातें मुझे कम पसंद थीं मैंने केशव को बतायी | उन्हें अच्छा
न भी लगा हो , तो भी उन्होंने जाहिर नहीं किया | कविता की प्रवृत्तियों पर बातचीत
होती रही | केशव भी तीव्र पसंद-नापसंद वाले व्यक्ति हैं | कविता की उनकी अपनी
धारणाएं हैं , जिनसे हमेशा सहमत होना कठिन है | खासकर ‘लोक’ को लेकर कुछ आत्यंतिक
आग्रह मुझे नहीं जंचता | ‘लोक’ आज की कविता में बहुत कुछ भावुकता का क्षेत्र बन
गया है | फिर भी केशव की धारणाओं से अलग , उनकी कवितायें मुझे पसंद हैं | वे लोक
को शरणस्थली कम ही बनाते हैं - आग्रह चाहे
जैसा भी हो |
अभी हाल में उन्होंने फोन पर एक कविता सुनायी --
‘औरंगजेब का मंदिर’ | इतने दिनों बाद उस यात्रा की स्मृति सजीव हो आयी | अवश्य
केशव ने अपने भीतर उस यात्रा की स्मृति को संजो रखा था | इससे एक कवि की मनोरचना
का परिचय मिलता है | शुक्ल जी कहते थे , कि केवन के मार्मिक स्थलों की पहचान कवि
की शक्ति होती है |
कविता ठीक-ठाक थी | बस , ठीक-ठाक | मैंने कुछ
सुझाव दिए | केशव ने कविता फिर से लिखी | उन्हें अपनी कविता से प्रेम तो है ,
लेकिन मोह नहीं , वरना उनके जैसा जिद्दी आदमी किसी आलोचक के कहने पर कविता सुधारने
को राजी हो , यह मुश्किल है | आखिरकार चौथे प्रारूप के बाद उन्होंने हथियार दाल
दिए , कि मेरे बस का और नहीं है ; जितना टटोलकर स्मृतियों से निकाल सकता था , वह
लिख दिया | यों , इसके बाद कविता में ‘और’ होना आवश्यक था – कम-से-कम केशव की रचना
प्रवृत्ति को देखते हुए | बहरहाल कविता इस प्रकार है -------
औरंगजेब का मंदिर
(बाला जी का मंदिर)
 |
| मुग़ल बादशाह 'औरंगजेब' |
यहाँ नहीं उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़
जह जुजबी ही भटक आते हैं इधर
जबकि एक रास्ता इधर से भी जाता है
एक बूढा पुजारी कपड़े में
लपेटे आलमगीर का फरमान
संदूकची में समेटे है
बड़े जतन से
इस बात का सबूत –
जिसे तारीख
जालिम कह नजीर देती है
उसका दिया भी कभी-न-कभी
धड़कता था दूसरों के लिए भी
महंथों मठाधीशों के बीच
परित्यक्त यह बूढा
यहाँ आपको बिना जात-पात पूछे
मिल सकता है उपलब्ध भोजन
आप छहाँ सकते हैं
इस पुरनिया पेड़ की छाँह में |
 |
| औरंगजेब द्वारा बनवाया मंदिर |
सैकड़ों साल पुरानी
मंदिर की दीवारों पर
टिका सकते हैं पीठ
गीता वेद रामायन श्रुतियों के साथ
एक साधु
लिए बैठा है एक बुतशिकन
बादशाह का फरमान
इतिहास की मोटी-मोटी किताबों में
तरह-तरह के मंतव्यों के बीच
यह पंद्रह लाईन का एक
अदना-सा-फरमान
तमाम धार्मिक उद्घोषों
जयकारों के बीच
धर्म और इतिहास के मुहाने से
पुकारती एक आवाज
तमाम ध्वंसावशेषों से क्षमा मांगती...
कोई सुने तो रूककर
एक आवाज यह भी है |
 |
| फरमान दिखाते पुजारी |
बिलकुल सच्चा वर्णन है | तथ्यपूर्ण और भावपूर्ण
| मंदिर के भीतरी परिवेश के चित्रण में जरुर कोताही की गयी है | विवरणों को लिखकर
रखने की आदत कवियों में जरा कम ही होती है | वे स्मृतियों और प्रभावों से काम चला
लेते हैं | इस मंदिर के जो अनुभव थे , यदि उनसे भीतरी वातावरण का चित्र कुछ और
समृद्ध होता , तो बेशक , अवसाद थोडा गहरा होता , लेकिन विडंबना का बोध अधिक तीव्र
होता | केशव अवसाद से ज्यादे जीवन-उल्लास के कवि हैं | केदार के प्रभाव और केशव की
‘लोक’ चेतना का यह अपना संश्लेष है | फिर भी मुझे संतोष है , कि केशव ने एक नयी
दिशा में प्रवेश किया |
शायद इतनी शिद्दत से विडम्बना के उद्घाटन में
केशव पहली बार लगे हैं | विडंबना वर्तमान तथ्य और ऐतिहासिक परंपरा , दोनों स्तरों
पर है | ‘एक रास्ता इधर से भी जाता है’ – यह मानो कविता का मूल स्वर है | यह
रास्ता अतीत और वर्तमान दोनों सन्दर्भों में एक विकल्प है | मुखर सन्देश के बजाय
गहरे विश्वास से केशव को यह स्वर मिला है | इसे ध्यान में रखिये , तब मालूम होगा
कि विडंबना कवि की किस करुणा से उपजी है | मंदिर का महंथ घृणा और आलोचना का पात्र
होता है ; लेकिन ‘यह बूढा’ अपने मंदिर की ही तरह परित्यक्त है | आलोचना का विषय
दयनीयता का विषय बन गया है | दूसरी तरफ इस मंदिर का निर्माण उस शासक ने किया था .
जिसकी ख्याति मंदिर तोड़ने के लिए थी | ‘एक बुतशिकन बादशाह’ ! इस प्रकार , दोहरी
विडंबना से केशव ने इस कविता का भावनात्मक ढांचा निर्मित किया है |
बद्ध संस्कार केवल वर्तमान के नहीं होते , अतीत
के भी होते हैं | केशव दोनों तरह की जड़ता से लड़ते हैं | उत्तर-आधुनिक पदावली में
कहें तो वे दोनों प्रकार की जड़ताओं का विखंडन करते हैं | लेकिन उत्तर-आधुनिकों की
भाँति विखंडन करके इति नहीं समझ लेते | उनकी दृष्टि गंभीर अर्थ में राजनीतिक है |
अच्छी बात यह है कि राजनीति यहाँ सतह पर नहीं है | इससे कविता का आतंरिक ढांचा
सुरक्षित रहता है | यह भावावेश का ऐसा विषय भी नहीं है , न ऐसा क्षण ही है , कि
कविता के ढाँचे को तोड़ा जाए | विषय यह मांग नहीं करता कि नागार्जुन-केदार जैसी
प्रत्यक्ष राजनीतिक शैली अपनाई जाए , और केशव की रचना-प्रवृत्ति भी सीधी राजनीतिक
अभिव्यक्ति के अनुरूप नहीं है | फिर भी , ‘एक आवाज यह भी है’ , कवि का यह विनम्र
स्वर सांप्रदायिक राजनीति के कोलाहल को ध्वस्त कर डालता है | यह मिथ्या पर आधारित
वैमनस्यपूर्ण राजनीति का , साम्प्रदायिक उद्देश्यों के लिए इतिहास के उपयोग की
कुटिलता का दृढ प्रतिवाद है |
उल्लेखनीय है कि यह प्रतिवाद अनायास अथवा आरोपित
नहीं है | कवि परस्पर-विरोधी तथ्यों को आमने –सामने रखता है | ‘इतिहास की
मोटी-मोटी किताबों’ और ‘तरह तरह के मंतव्यों’ के समानांतर सिर्फ ‘पंद्रह लाइनों का
एक अदना-सा फरमान’ है , जो पूरी ताकत से डट जाता है | इस फरमान में औरंगजेब का यह
ऐलान है कि शाही खजाने से बालाजी के इस मंदिर को हमेशा-हमेशा नियमित मदद की जाती रहेगी
| एक विडम्बना यह भी है , कि हमेशा-हमेशा के लिए खुद शहंशाह भी न रह पाए , मदद की
बात तो दूर रही !
कवि ही यह योग्यता रखता है , कि बद्ध संस्कारों
और आग्रहों से मुक्त रहकर प्रचार से ढकें सत्य को उभारे | औरंगजेब एक जालिम शासक
था , लेकिन मनुष्य भी था | केशव देखते हैं कि जालिम कहे गए शख्श का ‘दिल कभी-न-कभी
धड़कता था दूसरों के लिए’ | महानायक या खलनायक बनाने की जगह मानुष के रूप में देखना
कवि का काम है |
संभव है , अगर यह मंदिर भी दूसरे मंदिरों की तरह
मुसलमान शासक से न जुड़ा होता तो , यहाँ भी ‘ बिना जात-पात पूछे’ सबको खाना न मिलता
| पुजारी और महंथ अपनी परिचित छवि में नहीं हैं | धार्मिक या सांप्रदायिक अलगाव के
साथ-साथ बिरादरी वाद का अलगाव भी है | कविता दोनों प्रश्नों से टकराती है | अतीत
और वर्तमान , जाति और धर्म इनके जटिल प्रसंगों को केशव ने साधे हुए संकेतों में
व्यक्त कर दिया है | ‘लोक’ चेतना वाली बहुत-सी समकालीन कविता का आंतरिक फलक इतना
व्यापक नहीं होता | खुद केशव की बहुत सी कवितायें इतनी संश्लिष्ट अभिव्यक्ति नहीं
कर पाती | भावुकता और यथार्थ – दृष्टि में यह अंतर है |
इतिहास में एक सजीव शक्ति है | यह बात अगर
विद्वेष का प्रचार देखकर समझा जा सकता है , तो उस प्रचार का प्रतिवाद भी इतिहास के
जरिये किया जा सकता है , इस बात को केशव की यह कविता समझा देती है | केशव ने
इतिहास को वर्तमान में पकड़ा है | इसलिए कविता में इतिहास एक निरंतरता और विडंबना
के रूप में द्वंद्वात्मक रूप में आया है | ‘सैकड़ों साल पुरानी मंदिर की दीवारों पर
टिका सकते हैं पीठ’ – यहाँ पुरानापन मृत नहीं है ; बल्कि मरती परिपाटियों का अस्वीकार
है | निरंतरता इस बात में कि जाति – धर्म से परे संस्कृत का एक समावेशी रूप है ,
भले ही वह आज उपेक्षित हो ; विडंबना इस बात में कि बादशाह के रहने पर जो मंदिर धन
धन्य और आगंतुकों से भरा रहता , वह आज वीरान है | यह हमारे समय पर एक टिप्पड़ी भी
है |
'नया ज्ञानोदय' के नवम्बर-2012 अंक से साभार
'नया ज्ञानोदय' के नवम्बर-2012 अंक से साभार
परिचय और संपर्क
 |
| अजय तिवारी |
लेखक अजय तिवारी हिंदी के
प्रख्यात आलोचक हैं
बी- 30 , श्रीराम अपार्टमेंट्स
32 / 4 , द्वारिका , नयी दिल्ली , 110078
मो.न. – 09717170693
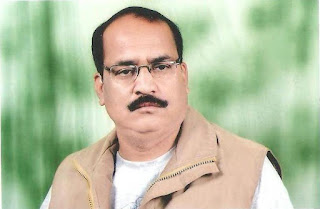




.jpg)